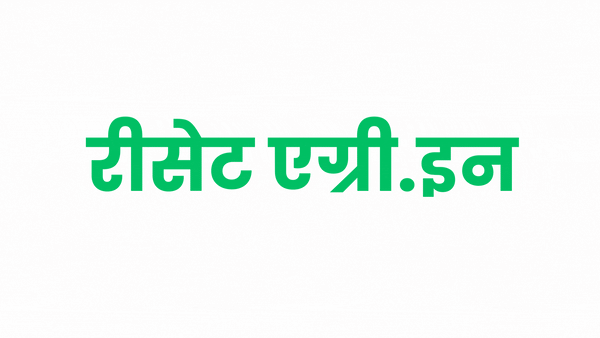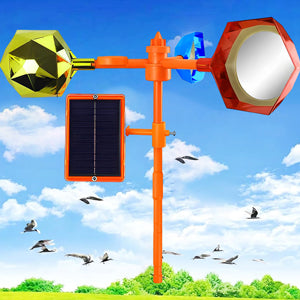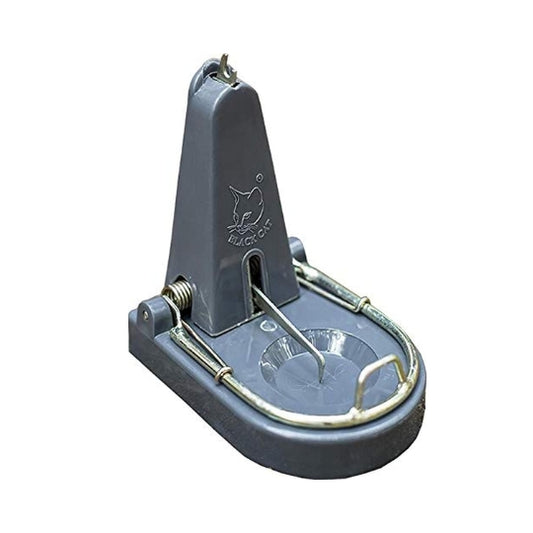पोषक मिटटी का घोल और फसल की उपज
Share
रिसेट एग्री किसान भाइयों का स्वागत करता है. किसान भाइयों, फसल के पोषण संतुलनका महत्व हम सब जानते है.
फसल के पोषण की बात करते ही हमारे दिमाग में यूरिया, डीएपी, एसएसपि, एनपीके, केल्शियम नायट्रेट, मैग्नेशियम सल्फेट,सल्फर, झिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मेंग्निज सल्फेट जैसे उर्वरकों के नाम घुमने लगते है. तो क्या यही सबकुछ है?
ऑर्गेनिक मेन्युअर, मृदा सुधारक, बेसल डोस, ड्रेंचींग, छिडकावके माध्यम से हमारी फसल में लागत (खर्चे) बढने लगती है. हर साल हम लोग हजारों रूपयेके खाद मिटटी में मिलाते है. कपनियों के संस्कारी एक्सपर्ट हमारे जहेन में "मिटटी में मिलाओ और सोना ऊगाओ" की संकल्पना ठूस ठूस के भरते है. फिर चाहे इनके खाद कितनेही मिलावटी क्यों ना हो!
- इतने सारे खादों का क्या होता है?
- क्या इतने सारे खादों की सचमुच जरूरत होती है?
- फसल के पोषण के आलावा इन खादों का हमारे मिटटी पर क्या असर होता है?
इन सारे सवालों को समझने के लिए हमे मिटटी के घोल को समझना होगा.
भारतीय किसान बनाम ग्रामीण विकास
छोटे किसानों के लिए सुधरे कृषि यंत्र
ओह रे! किसान
वाह रे किसान
कृषि विज्ञान और किसान
ग्रामीण कृषि मौसम विज्ञान
कृषक: संकट और समाधान
किसान की बेटी
लेटेस्ट टेक्नीकल बुक ऑन इन्सेक्टीसाइड्स एंड पेस्टीसाइड्स
कृषि सेवा केंद्र मार्गदर्शिका
मिटटी का घोल
बीजोंके अनुरण के बाद, जब बीजों में जमा सारा पोषण खत्म हो जाता है, पौध पूरी तरह सूरज और मिटटी पर निर्भर हो जाता है. ऊर्जा के अलावा, उसकी सारी जरूरते मिटटी ही पूर्ण करती है. गौरतलब है के मिटटी और मिटटी में बसे पोषक तत्व एकसमान नही होते. परिस्थती नुरूप उनमे परिवर्तन होता रहेता है.
यह पोषण तत्व कभी पानी में घुलते है, तो कभी पानी से निकलकर, अन्य स्वरूप में तब्दील हो जाते है. क्योंकि पौध सिर्फ अकार्बनिक (इनओरगेनिक) स्वरूप में ही पोषक तत्वों को सोख सकती है, अन्य सारे स्वरूप पौध के सीधे सीधे काम के नहीं होते.
अकार्बनिक स्वरूप में गतिशील पोषक तत्व पानी में जो घोल बनाते है उसे सोईल सोल्यूशन याने "मिटटी का घोल: कहा जाता है. यह "मिटटी का घोल" ही फसल के पोषण के लिए जिम्मेदार होता है. पोषक तत्वों का यह घोल बनता बिगड़ता रहेता है. इसके पोषक तत्व अलग अलग श्रोतोंसे आते है और अलग अलग स्वरूप में पानी से लुप्त हो जाते है. "मिटटी का घोल" किसी बर्तन में बनाया गया पानी का घोल नही है. यह एक पानी के पतली परत के रूप में जड़ोंके एव कार्बनि तत्वोंके पृष्ठभाग पर बनता-बिगड़ता रहेता है.
मिटटी खनिजों से बनी होती है. इन खनिजोंका जब अपक्षय/पतन होता है, प्रार्थमिक खनिज तत्व मिटटी के घोल में मिल जाते है. यह एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है. बंजर जमीन में ऐसे खनिज अधिक होते है. हर फसल के साथ खेतों के मिटटी में इनका प्रतिशत कम होते जाता है.
खनिजोंका अपक्षय होने की प्रक्रिया एकतरफ़ा होती है. मिटटी के घोल से यह खनिज जब अवक्षेपित होते है, इन्हें दुय्यम खनिज कहा जाता है. यह दुय्यम खनिज दुबारा मिटटी के घोल में घुलमिल सकते है.
आप जानते है के पौध का पोषण करने की क्षमता रखने वाला मिटटी का घोल केवल अकार्बनिक पोषण तत्वों का ही बना होता है. यह अकार्बनिक पोषक तत्व, मिटटी के घोल से निकलकर, कार्बनिक तत्वों से बने कणों के सलग्न हो सकते है और इस सलग्नता को खत्म कर फिरसे मिटटी के घोल में मिल सकते है. इसे हम धन और ऋण-भार विनिमय कहते है. मिटटी में ह्यूमस (ह्युमिक एसिड) जैसे कार्बनिक पोषक तत्व होते है जो अकार्बनिक पोषक तत्वों को मिटटी में बनाए रखते है.
पौधों के अलावा मिटटी में ढेर रसे सूक्ष्मजिव और सजीव होते है.इनमें से सारे सूक्ष्मजिव और कुछ सजिव् मिटटी से पोषक तत्व सोखते है. इनके द्वारा सोखे गये पोषक तत्व अब पौधों को सीधे उपलब्ध नही होते. लेकिन जब यह सूक्ष्मजीव और सजीव मरते है, इनमें बसे पोषक तत्व खनिजीकरण से फिरसे मिटटी के घोल में समाविष्ट हो सकते है. पौधे आपने जडोके क्षेत्र में सूक्ष्मजोवोको बसाने हेतु स्त्राव के माध्यम से कार्बनि पदार्थ छोडती है. इससे सूक्ष्मजीवोकी संख्या बढती है और वो मिटटी के पोषक तत्वोको पौध के लिए संजोके रखते है.
घोलसे बाहर निकल चुके तत्वोको फिरसे घोलमें लाने हेतु वनस्पति जड़ों से ऐसे रसायन छोडती है जो इन खनिजोंकों पकडकर मिटटी के घोल में घोलते है. इन्हें चिलेट/नखरिन या फायटोसिडेरोफोर कहा जाता है. फेरस, जिंक, मेंग्निज, कोपर जैसे तत्वों से पौधों का पोषण करने में इनका अहम महत्व है.
मिटटी के घोल से कुछ पोषक तत्व जैसे नायट्रेट, अमोनिया हवा में उड़ जाते है तो हवा से ऐसेही कुछ पोषण तत्व मिटटी के घोल में उरत आते है. पत्तों पर तथा जड़ोंपर बने गाठों में जीवाणु नत्र का स्थिरीकरण करते है. बिजली के कडकने से भी नत्र का स्थिरीकरण होता है जो बरसात के माध्यम से मिटटी के घोल में पहुच जाता है.
नायट्रेट और सल्फेट जैसे पोषक तत्व पानी के बहाव में मिलकर मिटटी की अन्धरुनी परतों में बहे जाते है. इसे लीचिंग भी कहा जाता है. इसके उल्टा कुछ पोषक तत्व गहरि मृदा से केशाकर्षन (केपिलरी एक्सन) से तथा मायक्रोरायझा के तंतुओ के माध्यम से मिटटी के घोल में वापिस आते है.
उपरोक्त जानकारी से हमे पता चलता है के अगर अचानक ही हम किसी खाद को एकसाथ मिटटी में मिलाए तो हो सकता है के इसका एक हिस्सा मिटटी के घोल के माध्यम से तुरंत फसल को उपलब्ध हो लेकिन अधिकतर हिस्सा या तो स्वरूप बदलकर मिटटी में बना रहेगा, या हवा में उड़ जाएगा, या उसका लीचिंग हो जाएगा. तो एक बात साफ़ है, कोईभी कितना भी कहे खादों को धीरे धीरे, छोटी छोटी किस्तोमे देना है.
पोषक एवं भरपूर उपज
मिटटी का घोल हमेशा पोषक तत्वों से भरा रहे इसलिए मिटटी में ह्यूमस या ह्युमिक एसिड जैसे कार्बनिक तत्वों का बना रहेना जरूरी है. संशोधन के आधार से पता चला है के औसत आधार पर हमारे मिट्टियों में कार्बनिक तत्व ०.१ प्रतिशत के आस पास है. इसे १ प्रतिशत से अधिक होना चाहिए. किसीभी मिटटी में जब कार्बनिक तत्व १२-१८ प्रतिशत के बिच में होता है उसे ओर्गेनीक मिटटी कहा जाता है. ऐसी ऑर्गेनिक मिटटी फसल पोषण के लिए उपयुक्त मानी जाती है.
एक एकड़ क्षेत्र के उपरी १ फिट परत में १७,९२,००० किलो मिटटी होती है. अगर इस एक फिट की परत में १ प्रतिशत कार्बनिक तत्व मिलाने के लिए १७९२० किलो ऑर्गेनिक मेन्युअर की जरूरत होगी. एक किलो मेन्युअर की कीमत सिर्फ ५ रूपये भी पकड़े तो इसका मूल्य करीबन ९० हजार रूपये होगा. अगर कार्बनिक तत्व १० प्रतिशत तक बढाना चाहेंगे तो इसकाखर्चा करीबन ९ से १० लाख प्रति एकड़ होगा. जाहिर तौर पर, व्यवहारिक स्वरूप में, कोईभी इतना खर्चा नही कर सकता!
इसीलिए किसानों को मिटटी में कार्बनतत्व बढाने का कार्य नियमित रूप से करना होगा.
पूरी तरह से सड़ी हुई खाद (गोबर, वर्मीकम्पोस्ट, सिटी कम्पोस्ट, फार्म यार्ड मेन्युअर) मिटटी में मिलाने से धन और ऋण-भार विनिमयकरने वाले कार्बनिक तत्व मिटटी में बने रहे सकते है.
कोयले के खदानों से मिलनेवाले पथरीले कोयले को सोडा/पोटेश लाय से गलाने पर ह्युमिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम संयुग प्राप्त होता है. सड़ी हुई खाद के कमी को पूरा करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है. मिटटी में मिलाने के बाद जब तक वह जडो के क्षेत्र में बना रहेता है, मिटटी के घोल को बनाए रखने का काम करते रहेता है. लेकिन वक्त के साथ या तो यह गल जाता है या लीचिंग होकर मिटटी के अंदरूनी परतों में चला जाता है. हम सबी जानते है के खदानी कोयले के कई उपयोग है और इससे ह्युमिक एसिड बनाने की प्रक्रिया काफी महँगी है. इसीलिए, ह्युमिक एसिड, ऑर्गेनिक मेन्युअर का पर्याय नही है, इसे फसल पोषण के दौरान प्रति एकड़ २ से ५ किलो तक इस्तेमाल किया जा सकता है. अधिक इस्तेमाल से कोई ख़ास लाभ नही होता है.
समुंदर में ढेर सारे खनिज होते है. इसीलिए समुद्री शेवाल को खनिजों की कोई कमी नही होती. इन समुद्रि शैवाल को निकालकर, साफ़ कर इससे खनिजों को निकाला जाता है. खनिज निकालने हेतु एसिड, अल्कली हायड्रोलिसिस, किण्वन जैसी प्रकियाए करनी पडती है. यह सारी प्रकियाए महँगी होती है और इसका ऑर्गेनिक मेन्युअर से कोई मुकाबला नही हो सकता.
फसल निकासी के बाद मिटटी में दबी हुई फसल की जड़े सड़कर मिटटी में कार्बनिक पदार्थो को बढाती है. इसी तरह अगर उपज के अलावा बचा हुआ फसल का हवा में झूलता हिस्सा अगर पतला (भुस्सा) कर मिटटी में मिलाया गया तो वह भी सडकर कार्बनि पदार्थो में तब्दिल हो जाता है.
मिटटी का कार्बन बढ़ाने का सबसे तार्किक तरीका है ढैंचा और मुंग की खेती. एक एकड़ में लगे फसल को लगभग 55 दिनों बाद खेतों में ही पलटाई व जुताई करने से औसतन 25 से 30 टन हरी खाद तैयार होती है. किसीभी फसल के बाद आवर्ती रूप से, अलटपलट कर ढैंचा और मुंग की उगाई, पलटाई व जुताई अवश्य करे.
उपरोक्त प्रक्रियाओं के दरम्यान, अपने आपे ही मिटटी में सूक्ष्मजीवों का बसेरा हो जाएगा. यह सूक्ष्म जिव असंख्य प्रकार के होंगे. जैविक खादों के मुकाबले यह कई गुना फायदेमंद होते है. गौरतलब है के इसके बाबजूद आप अझेटोबेक्टर, रायझोबीअम, पिएसबी, केएसबी, ट्रायकोडर्मा, शुडोमोनास, बेसिलस, बव्हेरिया, मेटारायझीअम जैसे सूक्ष्म जीवों के इस्तेमाल को नकार नही सकते. इनका उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में करना ही होगा. लेकिन सिर्फ इनके भरोसे आप मिटटी को उपजावू नही बना सकते.
जब मिटटी में पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन और सूक्ष्म जीवों की बहुतायत होगी तब इनमे फसलों के जड़ोद्वारा तथा सूक्ष्मजीवोंसे निकलने वाले चिलेटर /नखरिन / फायटोसिडेरोफोर की कोई कमी नही होगी. तो फसल को झिंक, लोह, मेंग्निज और कोपर जैसे सूक्ष्मघटकों की भी कोई कमी नही होगी. लेकिन बदलते परिवेश में कभी कभी इन घटकों के कमी के लक्षण फसल पर दिखाई दे सकते है, उपज घट सकती है. इसलिए सूक्ष्मअन्न द्रव्यों के मिश्रणों का उपयोग फसल के वृद्धि के दरम्यान तो करना ही होगा. गौरतलब है के इनकी जरूरत नाम मात्र ही रहेगी.
तो क्या एन-पि-के और केल्शियम, मैग्नेशियम और सल्फर खादों की भी जरूरत नहीं होंगी?
कपास, सोयबीन, मका, धान, गेहू, ज्वार, बाजरा, गन्ना, पपीता, आलू, बेंगन, मिर्च, टमाटर,खीरा, करेला, कद्दू जैसे फसलों के अधिक उपजाऊ प्रजातियों का इस्तेमाल करते हुए, उपज के माध्यम से नत्र, फोस्पेट, पोटेश, केल्शियम, मैग्नेशियम और सल्फर की निकासी बड़े तौर पर होती है. नत्र की निकासी की भरपाई तो फिरभी बिजली के कडकने से और जीवाणु ओ के स्थिरीकरण से अंशत: होती है, लेकिन अन्य घटकों के भरपाई के लिए हमे रासायनिक खादों पर पूर्णत: निर्भर रहेना ही होगा. अगर आप फसलों की कम उपज देने वाली प्रजातियों का इस्तेमाल करते हो तो आप रासायनिक खादों के इस्तेमाल को नकार सकते है. लेकिन ऐसे प्रजातियों के खेती को शौकिया किया जा सकता है. खुली अर्थव्यवस्थावाले आधुनिक युग में, जहा इंसानों की पैदाइश चरम पर है, शौकिया खेती सिर्फ घरोंके छत पर ही हो सकती है.
किसान भाइयों, आशा करता हु के यह लेख आपको पसंद आएगा. कोई शिकायत या शंका हो तो कमेंट में प्रश्न पूछे.
लेख को अवश्य शेअर करे.
धन्यवाद!